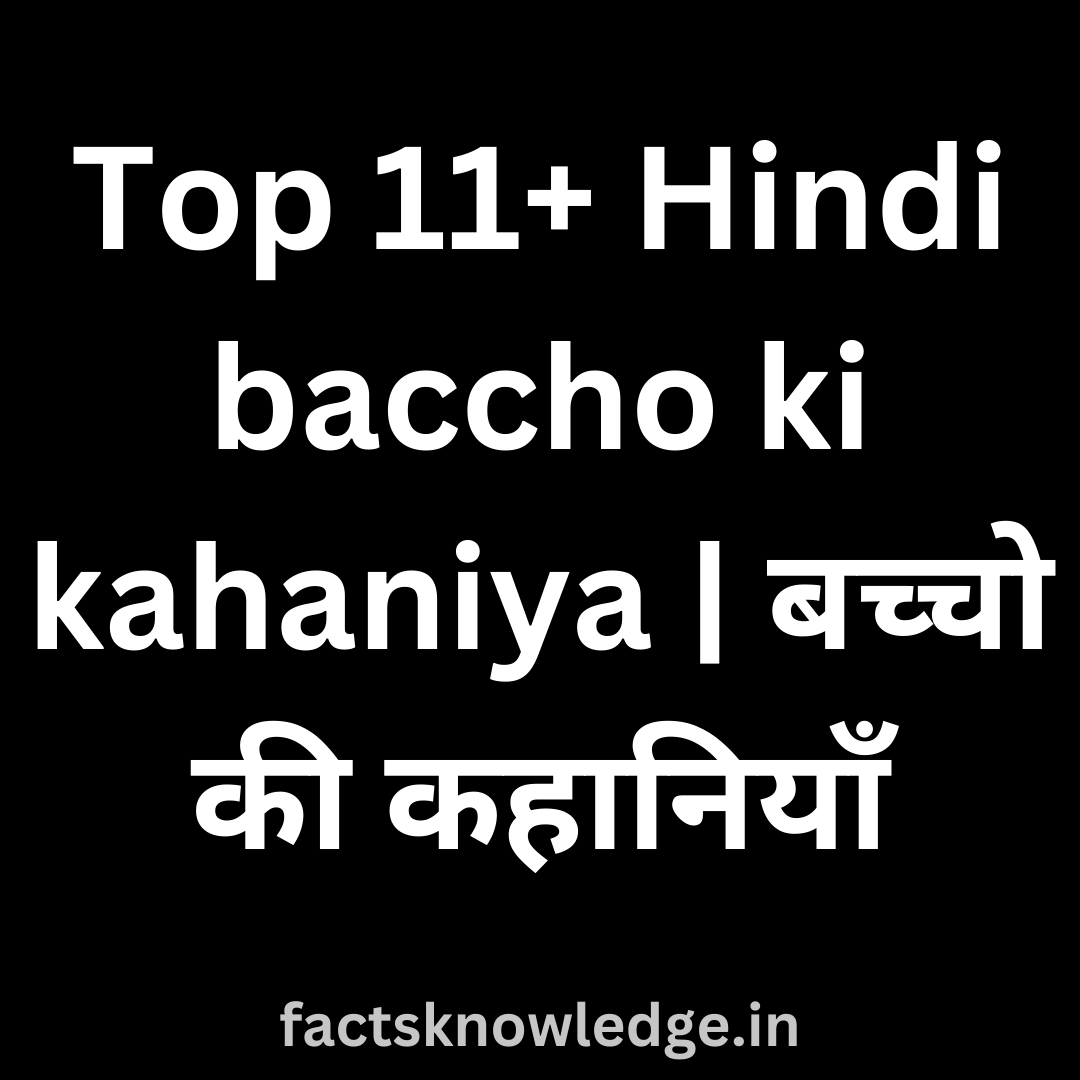बच्चो की कहानियाँ | Baccho ki kahaniya: फैक्ट्स नॉलेज के पास ढेर सारी बच्चो की कहानियाँ है पढ़ने के लिए और अपने बच्चो को सुनाने के लिए और अगर आप अपने स्कूल के कम्पीटीशन के लिए भी कहानियाँ ढूंढ रहे है तो आप एकदम सही जगह आये है।
बच्चो की कहानियाँ | दो मछलियों और एक मेंढक की कथा
एक तालाब में दो मछ़लियाँ रहती थीं । एक थी शतबुद्धि (सौ बुद्धियों वाली), दूसरी थी सहस्त्रबुद्धि (हजार बुद्धियों वाली) । उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था । उसका नाम था एकबुद्धि । उसके पास एक ही बुद्धि थी । इसलिये उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था । शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था।
एक दिन सन्ध्या समय तीनों तालाब के किनारे बात-चीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ़ मछि़यारे हाथों में जाल लेकर वहाँ आये । उनके जाल में बहुत सी मछ़लियाँ फँस कर तड़प रही थीं । तालाब के किनारे आकर मछि़यारे आपस में बात करने लगे । एक ने कहा – “इस तालाब में खूब मछ़लियाँ हैं, पानी भी कम है। कल हम यहाँ आकर मछ़लियां पकड़ेंगे ।”
सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहाँ आने का निश्चय करके मछि़यारे चले गये। उनके जाने के बाद सब मछ़लियों ने सभा की। सभी चिन्तित थे कि क्या किया जाय। सब की चिन्ता का उपहास करते हुये सहस्त्रबुद्धि ने कहा—“डरो मत, दुनियां में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाय।
सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते; इसीलिये संसार बना हुआ है । किसी के कथनमात्र से डरना कापुरुषों का काम है । प्रथम तो वह यहाँ आयेंगे ही नहीं, यदि आ भी गये तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सब की रक्षा करलूँगी ।”
शतबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा – “बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ़ संभव है। जहां वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहां बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथनमात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छो़ड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता । भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए ।”
तालाब की मछ़लियों को तो शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एकबुद्धि मेंढक ने कहा—“मित्रो ! मेरे पास तो एक ही बुद्धि है; वह मुझे यहां से भाग जाने की सलाह देती है । इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छो़ड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊँगा।”
यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया ।दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछि़यारे वहाँ आये । उन्होंने तालाब में जाल बिछा़ दिया । तालाब की सभी मछ़लियां जाल में फँस गईं । शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किन्तु मछि़यारे भी अनाड़ी न थे । उन्होंने चुन-चुन कर सब मछ़लियों को जाल में बांध लिया । सबने तड़प-तड़प कर प्राण दिये ।
सन्ध्या समय मछि़यारों ने मछ़लियों से भरे जाल को कन्धे पर उठा लिया । शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि बहुत भारी मछ़लियां थीं, इसीलिए इन दोनों को उन्होंने कन्धे पर और हाथों पर लटका लिया था । उनकी दुरवस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा-
“देख प्रिये ! मैं कितना दूरदर्शी हूं । जिस समय शतबुद्धि कन्धों पर और सहस्त्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एकबुद्धि इस छो़टे से जलाशय के निर्मल जल में सानन्द विहार कर रहा हूँ । इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊँचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्रबुद्धि की अपेक्षा एकबुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है ।”
संगीतमय गधा
एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपडों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। बस रात को चरने के लिए खुला छोड देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था।
एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा ‘कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं?’
गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पडता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर-उधर मुंह मारना पडता है।
गीदड़ बोला ‘तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहां पास में ही एक बडा सब्जियों का बाग़ है। वहां तरह-तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। खीरे, ककडियां, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग़ तोडकर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छककर खाता हूं और सेहत बना रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आया करो।’ लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया।
बाग़ में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग़ में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया।
उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते। बाग़ में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे-धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फडफडाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा ‘मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक हैं?’
गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला ‘मेरा दिल गाने का कर रहा हैं। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढैंचू राग गाऊं।’
गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी ‘न-न, ऐसा न करना गधे भाई। गाने-वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहां चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्यौता मत दो।’
गधे ने टेढी नजर से गीदड़ को देखा और बोला ‘गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो?’
गीदड़ ने हाथ जोडे ‘मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। केवल अपनी जान बचाना जानता हूं। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की ज़िद छोडो, उसी में हम दोनों की भलाई है।’
गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा ‘तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता।’
गीदड़ बोला ‘गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो। बाग़ के चौकीदार जाग जाएंगे।’
गधा हंसा ‘अरे मूर्ख गीदड़! मेरा राग सुनकर बाग़ के चौकीदार तो क्या, बाग़ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा।’
गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोडकर बोला ‘गधे भाई, मुझे अपनी ग़लती का अहसास हो गया हैं। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूं। मेरे जाने के दस मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं।’
गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाग़ के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लट्ठ लेकर दौडे, जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला “यही है वह दुष्ट गधा, जो हमारा बाग़ चर रहा था।’
बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पडे। कुछ ही देर में गधा पिट-पिटकर अधमरा गिर पडा।
सीख- अपने शुभचिन्तकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।
ब्राह्मण का सपना
एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था । उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोडे़ से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था । उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उसपर लेटे-लेटे विचित्र सपने लेने लगा, और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा ।
उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य १०० रुपये हो जायगा । उन सौ रुपयों से मैं दो बकरियां लूँगा । छः महीने में उन दो बकरियों से कई बकरियें बन जायंगी । उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा । गौओं के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा ।
घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जायगा । सोना बेचकर मैं बहुत बडा़ घर बनाऊँगा । मेरी सम्पत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरुपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा । वह मेरी पत्नी बनेगी । उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा ।
जब वह घुटनों के बल चलना सीख जायेगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे़ की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल-लीलायें देखूंगा । उसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर मां की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आयेगा तो मैं उसकी मां को क्रोध से कहूँगा—“अपने बच्चे को संभाल ।”
वह गृह-कार्य में व्यग्र होगी, इसलिये मेरा वचन न सुन सकेगी । तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारुंगा । यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिये ऊपर उठा । वह ठोकर सत्तु-भरे घड़े को लगी । घड़ा चकनाचूर हो गया । कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गये ।
दो सिर वाला जुलाहा
एक बार मन्थरक नाम के जुलाहे के सब उपकरण, जो कपड़ा बुनने के काम आते थे, टूट गये । उपकरणों को फिर बनाने के लिये लकड़ी की जरुरत थी । लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्रतट पर स्थित वन की ओर चल दिया।
समुद्र के किनारे पहुँचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जायेंगे । यह सोच कर वृक्ष के तने में वह कुल्हाडी़ मारने को ही था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उसे कहा—-“मैं इस वृक्ष पर आनन्द से रहता हूँ, और समुद्र की शीतल हवा का आनन्द लेता हूँ । तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं । दूसरे के सुख को छी़नने वाला कभी सुखी नहीं होता ।”
जुलाहे ने कहा —-“मैं भी लाचार हूँ । लकड़ी के बिना मेरे उपकरन नहीं बनेंगे, कपड़ा नही बुना जायगा, जिससे मेरे कुटुम्बी भूखे मर जायेंगे । इसलिये अच्छा़ यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो, मैं इस वृक्ष की शाखायें काटने को विवश हूँ ।”
देव ने कहा—-“मन्थरक ! मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ । तुम कोई भी एक वर माँग लो, मैं उसे पूरा करुँगा, केवल इस वृक्ष को मत काटो ।”
मन्थरक बोला—-“यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो । मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुम से वर मांगूंगा ।”
देव ने कहा—“मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करुँगा ।”
गाँव में पहुँचने के बाद मन्थरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई । उसने उससे पूछा़—-“मित्र ! एक देव मुझे वरदान दे रहा है, मैं तुझ से पूछ़ने आया हूँ कि कौन सा वरदान माँगा जाए ।”
नाई ने कहा—-“यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले । मैं तेरा मन्त्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे ।”
तब, मन्थरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही । नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मन्त्रणा करना नीति-विरुद्ध बतलाया । उसने सम्मति दी कि “स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायणा होती हैं । अपने सुख-साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ़ भी सूझ नहीं सकता । अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है, तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है ।”
मन्थरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किये बिना कुछ़ भी न करने का विचार प्रकट किया । घर पहुँचकर वह पत्नी से बोला— “आज मुझे एक देव मिला है । वह एक वरदान देने को उद्यत है । नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाय । तू बता कि कौन सी चीज़ मांगी जाये ।”
पत्नी ने उत्तर दिया—“राज्य-शासन का काम बहुत कष्ट-प्रद है । सन्धि-विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता । राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है । ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे ।”
मन्थरक ने कहा —“प्रिय ! तुम्हारी बात सच है, राजा राम को और राजा नल को भी राज्य-प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था । हमें भी कैसे मिल सकता है ? किन्तु प्रश्न यह है कि राज्य न मांग जाय तो क्या मांगा जाये ।”
मन्थरक-पत्नी ने उत्तर दिया—“तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो, उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है । यदि तुम्हारे हाथ दो की जगह चार हों और सिर भी एक की जगह दो हों तो कितना अच्छा़ हो । तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जायगा । इससे समाज में हमारा मान बढे़गा ।
मन्थरक को पत्नी की बात जच गई । समुद्रतट पर जाकर वह देव से बोला—“यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दो कि मैं चार हाथ और दो सिर वाला हो जाऊँ ।”
मन्थरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया । उसके दो सिर और चार हाथ हो गये । किन्तु इस बदली हालत में जब वह गाँव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया, और राक्षस-राक्षस कहकर सब उसपर टूट पड़े ।
वानरराज का बदला
एक नगर के राजा चन्द्र के पुत्रों को बन्दरों से खेलने का व्यसन था । बन्दरों का सरदार भी बड़ा चतुर था । वह सब बन्दरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था । सब बन्दर उसकी आज्ञा का पालन करते थे । राजपुत्र भी उन बन्दरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे ।
उसी नगर के राजगृह में छो़टे राजपुत्र के वाहन के लिये कई मेढे भी थे । उन में से एक मेढा बहुत लोभी था । वह जब जी चाहे तब रसोई में घुस कर सब कुछ खा लेता था । रसोइये उसे लकड़ी से मार कर बाहिर निकाल देते थे ।वानरराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिन्तित हो गया।
उसने सोचा ’यह कलह किसी दिन सारे बन्दरसमाज के नाश का कारण हो जायगा कारण यह कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढा घुड़साल में घुस कर आग लगा देगा । इससे कई घोड़े जल जायंगे । जलन के घावों को भरने के लिये बन्दरों की चर्बी की मांग पैदा होगी । तब, हम सब मारे जायंगे ।’
इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बन्दरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें । किन्तु उस समय बन्दरों ने उसकी बात को नहीं सुना । राजगृह में उन्हें मीठे-मीठे फल मिलते थे । उन्हें छोड़ कर वे कैसे जाते ! उन्होंने वानरराज से कहा कि “बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मन्द पड़ गई है । हम राजपुत्र के प्रेम-व्यवहार और अमृतसमान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जायंगे ।”
वानरराज ने आंखों में आंसू भर कर कहा —“मूर्खो ! तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते । यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ।” यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छो़ड़्कर वन में चला गया ।
उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिस से वानरराज ने वानरों को सावधान किया था । एक लोभी मेढा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फैंकी । मेढे के बाल जलने लगे । वहाँ से भाग कर वह अश्वशाला में घुस गया । उसकी चिनगारियों से अश्वशाला भी जल गई । कुछ़ घोड़े आग से जल कर वहीं मर गये । कुछ़ रस्सी तुड़ा कर शाला से भाग गये ।
तब, राजा ने पशुचिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिये कहा । वैद्यों ने आयुर्वेदशास्त्र देख कर सलाह दी कि जले घावों पर बन्दरों की चर्बी की मरहम बना कर लगाई जाये । राजा ने मरहम बनाने के लिये सब बन्दरों को मारने की आज्ञा दी । सिपाहियों ने सब बन्दरों को पकड़ कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया ।
वानरराज को जब अपने वंश-क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुःखी हुआ । उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी । दिन-रात वह इसी चिन्ता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन मेम ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे।
उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गये, सब मर गये; कोई वापिस नहीं आया । वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है । उसका पता लगाने के लिये उसने एक उपाय किया । कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगा कर पानी पीना शुरु कर दिया ।
थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किये हुए मगरमच्छ निकला । उसने कहा—“इस तालाब में पानी पीने के लिये आ कर कोई वापिस नहीं गया, तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है । मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ । तू जो वर मांगेगा, मैं दूंगा । कोई सा एक वर मांग ले ।”
वानरराज ने पूछा —-“मगरराज ! तुम्हारी भक्षण-शक्ति कितनी है ?”
मगरराज—-“जल में मैं सैंकड़ों, सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ; भूमि पर एक गीडड़ भी नहीं ।”
वानरराज—-“एक राजा से मेरा वैर है । यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ ।”
मगरराज ने कंठहार दे दिया । वानरराज कंठहार पहिनकर राजा के महल में चला गया । उस कंठहार की चमक-दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा । राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा—“वानरराज ! यह कंठहार तुम्हें कहाँ मिला ?”
वानरराज—-“राजन् ! यहाँ से दूर वन में एक तालाब है । वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगायगा उसे वह कंठहार मिल जायगा ।”
राजा ने इच्छा प्रगट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिस से सब को एक-एक कंठहार की प्राप्ति हो जायगी ।”
निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुँच गये । किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता । तृष्णा सबको अन्धा बना देती है । सैंकड़ों वाला हजा़रों चाहता है; हजा़रों वाला लाखों की तृष्णा रखता है; लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है । मनुष्य का शरीर जराजीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है । राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई ।
सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए । वानरराज ने राजा से कहा—“आप थोड़ा ठहर जायं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिये । आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजियेगा । हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे ।”
जितने लोग जलाशय में गये, सब डूब गये; कोई ऊपर न आया । उन्हें देरी होती देख राजा ने चिन्तित होकर वानरराज की ओर देखा । वानरराज तुरन्त वृक्ष की ऊँची शाखा पर चढ़कर बोला—-“महाराज ! तुम्हारे सब बन्धु-बान्धवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है । तुम ने मेरे कुल का नाश किया था; मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया । मुझे बदला लेना था , ले लिया । जाओ, राजमहल को वापिस चले जाओ ।”
राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किन्तु अब कोई उपाय नहीं था । वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था । हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है ।
राजा के वापिस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला । उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की ।
राक्षस का भय
एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रुपवती थी। उसे हर समय यही डर
रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न करले । उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी । रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था ।
एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया । घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छि़पा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है “यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर ।”
राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा, जिससे राजकुमारी इतनी डरती है । किसी तरह यह जानना चाहिये कि वह कैसा है ? कितना बलशाली है ?
यह सोचकर वह घोड़े का रुप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा ।
उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राज-महल में आया । वह वहाँ घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था । अश्वशाला में जा कर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरुपी राक्षस को ही सबसे सुन्दर घोड़ा देखकर वह उसकी पिठ पर चढ़ गया । अश्वरुपी राक्षस ने सम्झा कि अवश्यमेव यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है । किन्तु अब कोई चारा नहीं था । उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी । चोर के हाथ में चाबुक थी । चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ ।
कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया । उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया । तब, चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है, जो मुझे मारना चाहता है । किसी ऊबड़-खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा । मेरी हड्डी-पसली टूट जायेगी ।
यह सोच ही रहा था कि सामने वटवृक्ष की एक शाखा आई । घोड़ा उसके नीचे से गुजरा । चोर ने घोडे़ से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया । घोड़ा नीचे से गुज़र गया, चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया ।
उसी वृक्ष पर अश्वरुपी राक्षस का एक मित्र बन्दर रहता था । उसने डर से भागते हुये अश्वरुपी राक्षस को बुलाकर कहा—
“मित्र ! डरते क्यों हो ? यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि मामूली मनुष्य है । तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हज़म कर लो ।”
चोर को बन्दर पर बड़ा क्रोध आ रहा था । बन्दर उससे दूर ऊँची शाखा पर बैठा हुआ था । किन्तु उसकी लम्बी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी । चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींच कर चबाना शुरु कर दिया । बन्दर को पीड़ा तो बहुत हुई लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिये वह वहाँ बैठा ही रहा । फिर भी, उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी।
उसे देखकर राक्षस ने कहा – “मित्र ! चाहे तुम कुछ ही कहो, किन्तु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गये हो ।”यह कह कर वह भाग गया ।
जातक कथाएँ
जातक या जातक पालि या जातक कथाएँ बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथायें हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में गिना जाता है जिसमे लगभग 600 कहानियाँ संग्रह की गयी है। इन कथाओं मे मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है।
चूंकि ‘जातक कथाएँ’ भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म सम्बन्धी कथाएँ है इसलिए अधिकतर कहानियों में वे ही प्रधान पात्र के रूप में चित्रित है। कहानी के वे स्वयं नायक है। कहीं-कहीं उनका स्थान एक साधारण पात्र के रूप में गौण है और कहीं-कहीं वे एक दर्शक के रूप में भी चित्रित किये गये हैं।
प्रायः प्रत्येक कहानी का आरम्भ इस प्रकार होता है-‘‘एक समय राजा ब्रह्मदत्त के वाराणसी में राज्य करते समय (अतीते वाराणसिंय बह्मदत्ते रज्ज कारेन्ते) बोधिसत्व कुरंग मृग की योनि से उत्पन्न हुए अथवा … सिन्धु पार के घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए अथवा ….. बोधिसत्व ब्रह्मदत्त के अमात्य थे अथवा ..बोधिसत्व गोह की योनि सें उत्पन्न हुए आदि, आदि।
रुरु मृग की कथा
रुरु एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन; माणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आँखें तथा तराशे स्फटिक-से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकडियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता।
जाहिर है कि रुरु एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुन्दरता उसकी विशेषता थी। लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था ; और मनुष्य की तरह बात-चीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावत: एक लोभी प्राणी है और लोभ-वश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है।
फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा-भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरु की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रुरु जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनायी दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना-स्थल पर पहुँचा तो उसने वहाँ की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया।
रुरु की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने कि सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरु के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रुरु उसे झटक कर अलग कर सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया।
सुरक्षित आदमी ने जब रुरु को धन्यवाद देना चाहा तो रुरु ने उससे कहा, “अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण-मृग है; क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्सन्देह मेरा शिकार करना चाहेंगे।” इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुरु पुन: अपने निवास-स्थान को चला गया।
कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुरु साक्षात् दर्शन कर लिए। रुरु की सुन्दरता पर मुग्ध; और हर सुन्दर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरु को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरु को ढूँढकर लाने का आग्रह किया।
सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई-भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूँढने में सहायक होगा उसे वह एक गाँव तथा दस सुन्दर युवतियाँ पुरस्कार में देगा।
राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरु ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरु का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गँवाये वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुँचा। फिर हाँफते हुए उसने रुरु का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला।
राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुँचे और रुरु के निवास-स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रुरु को रानी की बतायी छवि के बिल्कुल अनुरुप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रुरु उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रुरु ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा “राजन् ! तुम मुझे मार डालो मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ ?”
उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुरु ने बचायी थी। रुरु के मुख से तभी यह वाक्य हठात् फूट पड़ा
“निकाल लो लकड़ी के कुन्दे को पानी से
न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को।”
राजा ने जब रुरु से उसके संवाद का आशय पूछा तो रुरु ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाये जाने की पूरी कहानी कह सुनायी। रुरु की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतध्नता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की।
रुरु की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुरु ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुन: अपने निवास-स्थल को लौट गया।
Baccho ki kahaniya in hindi
मानसरोवर, आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानस-सरोवर’ के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुन्दर नर्तकियों की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रुप से गुणवान और शीलवान भी थे।
फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालान्तर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण-सौन्दर्य का ज्ञान होने लगा।
वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उस के मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस-सदृश एक मनोरम-सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुण्डरीक, सौगन्धिक, तमरस और कहलर विकसित करवाये।
मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियाँ भी वहाँ बसायी गयीं। साथ ही राजा ने वहाँ बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवायी, जिससे दूर-दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहाँ विचरण करने लगे।
एक बार, वर्षा काल के बाद जब हेमन्त ॠतु प्रारम्भ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुन्दरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गयी।
तत्काल वे नीचे उतर आये और महीनों तक वहाँ की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अन्ततोगत्वा वर्षा ॠतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गये। मानस पहुँच कर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे।
हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए, यह कहा कि, पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है। वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं। किन्तु जन्तु जो कहलाता है “मानव” बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत।
फिर भी कुछ दिनों के बाद हंस-राज को हंसों की ज़िद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ॠतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया।
एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाये गये जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी-हंसों को तत्काल वहाँ से प्रस्थान करने को कहा जिससे मानस के सारे हंस वहाँ से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गये।
रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति-सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुँचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था।
निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामि-भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था; किन्तु मानव-धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया।
दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निस्सन्देह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख़शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अत: तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गये और उसे राजा के पास चलने को कहा।
निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज-दरबार पहुँचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गये। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही उसके पास आ गये थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राज-दण्ड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राजदरबार में सादर सुनता रहा।
इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुन: मानस को वापिस लौट गये।
चाँद पर खरगोश
गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके तीन मित्र थे – बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोसथ के दिन परम-दान का निर्णय लिया क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। (उपोसथ बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है)
जब उपोसथ का दिन आया तो सुबह-सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने-अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी सात लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा, अपने घर को लौट आया। उछलता-कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़, अपने घर ले आया।
तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया। किन्तु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात् घास-पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अत: उसने उपोसथ के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया।
उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्माण्ड को दोलायमान करने लगा और सक्क के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परम्परा में सक्क को शक्र या इन्द्र कहते हैं। सक्क ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रुप में वह उन चारों मित्रों की दान-परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे।
ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने सक्क को अपने-अपने घरों से क्रमश: मछलियाँ; मांस और दही ; एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा। किन्तु सक्क ने उनके द्वारा दी गयी दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की।
खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलायी गयी तो उसने तीन बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएँ। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा।
सक्क उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी।
हाँ, आश्चर्य ! आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी; सक्क के द्वारा किये गये परीक्षण का एक माया-जाल था।
सम्मोहित सक्क ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल, चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा,
“जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश ! जगत् तुम्हारी दान-वीरता को याद रखेगा।”
छद्दन्द हाथी की कहानी
हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियाँ हुआ करती थीं – छद्दन्त और उपोसथ। छद्दन्त हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके छ: दाँत होते थे। (ऐसा पालि साहित्य मे उल्लिखित है।) छद्दन्त हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी दो रानियाँ थी – महासुभद्दा और चुल्लसुभद्दा।
एक दिन गजराज और उसकी रानियाँ अपने दास-दासियों के साथ एक सरोवर में जल-क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल-वृक्ष भी था। गजराज ने खेल-खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्दा को आच्छादित कर गये।
किन्तु वृक्ष की सूखी टहनियाँ और फूल चुल्लसुभद्दा के ऊपर गिरे। चुल्लसुभद्दा ने इस घटना को संयोग न मान, स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। तत: छद्दन्तराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली।
कालान्तर में चुल्लसुभद्दा मर कर मद्द राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरान्त वाराणसी की पटरानी। किन्तु छद्दन्तराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्दन्तराज के दन्त प्राप्त करने को उकसाया। फलत: राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया।
सात वर्ष, सात महीने और सात दिनों के पश्चात् सोनुत्तर छद्दन्तराज के निवास-स्थान पर पहुँचा। उसने वहाँ एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढ्ँक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्दन्तराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने उस पर विष-बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्दन्त ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को हाथ में धनुष लिये देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा।
किन्तु सोनुत्तर ने संन्यासियों का गेरुआ वस्र पहना हुआ था जिस के कारण गजराज ने निषाद को जीवन-दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का हृदय-परिवर्तन हुआ। भाव – विह्मवल सोनुत्तर ने छद्दन्त को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ आया था।
चूँकि छद्दुंत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था इसलिए छद्दुंत ने मृत्यु-पूर्व स्वयं ही अपनी सूँड से अपने दांत काट कर सोनुत्तर को दे दिये।वाराणसी लौट कर सोनुत्तर ने जब छद्दन्त के दाँत रानी को दिखलाये तो रानी छद्दन्त की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गयी।
महाकपि के बलिदान की कहानी
हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से- कहानियों तक ही सिमट कर रह गयी हैं। यह कहानी उस समय की है, जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी।
उस पेड़ पर वानरों का एक झुण्ड रहता था, जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बन्दरों की तुलना कई गुणा ज्यादा बड़ा, बलवान्, गुणवान्, प्रज्ञावान् और शीलवान् था, इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था।
अपनी दूर-दृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्तव दिया क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिर कर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता।
एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों-बीच पक कर टहनी से टूट, बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया।
उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों दास-दासीयों तथा के साथ उसी नदी की तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगन्ध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आँखें बंद कर आनन्दमग्न हो गयीं। राजा भी उस सुगन्ध से आनन्दित हो उठा।
शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगन्ध के स्रोत के पीछे दौड़ाये। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूँढ लिया। किन्तु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहाँ रास नहीं आयी। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारम्भ कर दिया।
वीर्यवान् महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेंत की लकड़ी को अपने पैरों से फँसा कर, फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्ला कर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूद कर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूद कर भाग गये।
राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा । उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिन्दा पकड़ लाने की आज्ञा दी।
उस समय महाकपि की हालत अत्यन्त गंभीर थी। साथी वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्थता भी करवायी, मगर महाकपि की आँखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं।
लक्खण मृग की कथा
हजारों साल पहले मगध जनपद के एक निकटवर्ती वन में हजार हिरणों का एक समूह रहता था जिसके राजा के दो पुत्र थे- लक्खण और काल। जब मृगराज वृद्ध होने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रत्येक के संरक्षण में पाँच-पाँच सौ मृग प्रदान किए ताकि वे सुरक्षित आहार-विहार का आनंद प्राप्त कर सकें।
उन्हीं दिनों फसल काटने का समय भी निकट था तथा मगधवासी अपने लहलहाते खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम और खाइयों का निर्माण कर रहे थे। मृगों की सुरक्षा के लिए वृद्ध पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने मृग-समूहों को लेकर किसी सुदूर और सुरक्षित पहाड़ी पर जाने का निर्देश दिया।
काला एक स्वेच्छाचारी मृग था। वह तत्काल अपने मृगों को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि लोग सूरज की रोशनी में उनका शिकार भी कर सकते थे। फलत: रास्ते में ही उसके कई साथी मारे गये।
लक्खण एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध मृग था। उसे यह ज्ञान था कि मगधवासी दिन के उजाले में उनका शिकार भी कर सकते थे। अत: उसने पिता द्वारा निर्दिष्ट पहाड़ी के लिए रात के अंधेरे में प्रस्थान किया। उसकी इस बुद्धिमानी से उसके सभी साथी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुँच गए।
चार महीनों के बाद जब लोगों ने फसल काट ली तो दोनों ही मृग-बन्धु अपने-अपने अनुचरों के साथ अपने निवास-स्थान को लौट आये। जब वृद्ध पिता ने लक्खण के सारे साथियों को जीवित और काला के अनेक साथियों के मारे जाने का कारण जाना तो उसने खुले दिल से लक्खण की बुद्धिमत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
संत भैंसा और नटखट बंदर की कथा
हिमवंत के वन में कभी एक जंगली भैंसा रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार। किंतु वह एक शीलवान भैंसा था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था। मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था।
अत: स्वभावत: वह भैंसा को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता; कभी उसे घास चरने से रोकता तो कभी उसके सींगों को पकड़ कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परम्पराओं में यमराज की सवारी भैंसा बतलाई जाती है।
उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदन की छेड़खानी बिल्कुल पसन्द न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसा को प्रेरित किया क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु भैंसा ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुँचाना शीलत्व नहीं है; और दूसरों को चोट पहुँचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। अत: बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा।
और एक दिन ऐसा ही हुआ जबकि वह भैंसा घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले भैंसा के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुँचा। बंदर ने आव देखी न ताव। पूर्ववत् वह दूसरे भैंसा के ऊपर चढ़ने की वैसी ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे भैंसा ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिये और पैरों से उसे रौंद डाला । क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गये।
सीलवा हाथी और लोभी मित्र की कथा
कभी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आँखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह अस्सी हज़ार गजों का राजा भी था।
वन में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सीलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आयी। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। अत: वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सीलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया।
सीलवा ने ज्योंही पैर फिर आगे बढ़ाया वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके वह आदमी भी रुक गया तीन बार जब सीलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दो हराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भीक हो कर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सीलवा ने तब उसके पास पहुँचा कर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा।
आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीलवा ने उसे तब अपनी सूँड के उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास-स्थान पर ले जाकर नानाप्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंतत: जब उस आदमी की भूख-प्यास का निवारण हो गया तो सीलवा ने उसे पुन: अपनी पीठ पर बिठा कर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया।
वह आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाज़ार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दाँत का सौदा कर आया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबन्ध कर सीलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया।
जब वह व्यक्ति से सीलवा के सामने पहँचा तो सीलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दाँतों की याचना की। उन दिनों सीलवा दान-पारमी होने की साधना कर रहा था। अत: उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दाँत काट सके।
उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सीलवा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पायी। मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गयी। वह महीने भर में फिर सीलवा के पास पहुँच कर उसके शेष दांतों की याँचना कर बैठा। सीलवा ने उस पुन: अनुगृहीत किया।
कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से सीलवा के पास पहुँचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दान-परायण सीलवा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था? क्षण भर में वह आदमी सीलवा के मसूढ़ों को काट-छेद कर उसके सारे दांत-समूल निकाल कर और अपने गन्तव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया।
खून से लथपथ दर्द से व्याकुल कराहता सीलवा फिर जीवित न रह सका और कुछ समयोपरान्त दम तोड़ गया।
लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था तभी घरती अचानक फट गयी और वह आदमी काल के गाल में समा गया।
तभी वहाँ वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया।
बुद्धिमान् वानर की कथा
हज़ारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह हज़ार बंदरों का राजा भी था।
एक दिन वह और उसके साथी वन में कूदते-फाँदते ऐसी जगह पर पहुँचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नयी जगह और नये परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी।
कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूद कर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देख कर वानरराज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नये स्थान से अनभिज्ञ था। अत: उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पदचिह्मों को देखा जो जलाशय को उन्मुख तो थे मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे।
बुद्धिमान् वानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्य-वास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गये। तब बुद्धिमान वानर ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेंत के जंगल थे जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क-सुड़क कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली।
सुनहरे पँखों वाले हँस की कहानी
वाराणसी में कभी एक कर्त्तव्यनिष्ठ व शीलवान् गृहस्थ रहा करता था । तीन बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा-सा घर संसार था । किन्तु अल्प-आयु में ही उसका निधन हो गया ।
मरणोपरान्त उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रुप में हुआ । पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य-योनि के घटना-क्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया । पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था । एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला जहाँ उसकी पूर्व-जन्म की पत्नी और तीन बेटियाँ रहा करती थीं ।
घर के मुंडेर पर पहुँच कर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा क्योंकि उसके मरणोपरान्त उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी । उसकी पत्नी और बेटियाँ अब सुंदर वस्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं । वैभव के सारे सामान भी वहाँ से तिरोहित हो चुके थे । फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापिस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें ।
इस घटना के पश्चात् हँस समय-समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख दे कर जाता था।
बेटियाँ तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाये। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही। मगर उसकी बेटियाँ ने उसका कड़ा विरोध किया।
अगली बार जब वह हंस वहाँ आया तो संयोगवश उसकी बेटियाँ वहाँ नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल-प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी-खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या। उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे।
बेटियाँ जब लौट कर घर आयीं तो उन्होंने अपने पूर्व-जन्म के पिता को खून से सना देखा; उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा-शुश्रुषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया।
स्वभावत: उसके पंख फिर से आने लगे। मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गये कि वह उडने के लिए समर्थ हो गया। तब वह उस घर से उड़ गया। और कभी भी वाराणसी में दुबारा दिखाई नहीं पड़ा।
बच्चो की कहानियाँ
- Small panchatantra short stories in hindi with moral
- पौराणिक हिंदी कहानियां
- 10 मजेदार कहानियां
- छोटी रोचक कहानियाँ
- 10 lines short stories with moral in Hindi
- Small short stories with moral values in hindi